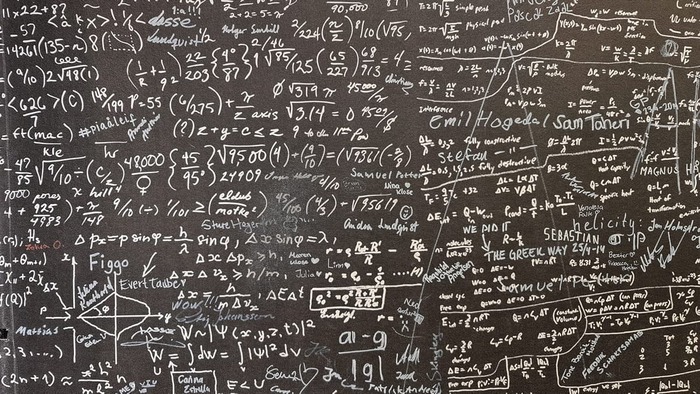
प्रेरणा
आज यहाँ विभिन्न स्थानों से, यहाँ तक कि तिब्बत से भी, बहुत से लोग आए हैं और आप सभी धर्म सम्बन्धी शिक्षाएँ सुनने आए हैं। इसलिए, बोधिचित्त संकल्प के विकास आदि के संबंध में, मैं यहाँ बोधगया में तोग्मेज़ांगपो द्वारा रचित 37 बोधि साधनाएँ और जे त्सोंगखापा द्वारा रचित पथ के तीन प्रमुख पहलुओं पर शिक्षा दूँगा। चूँकि हम एक अत्यंत पवित्र स्थान पर हैं, इसलिए यहाँ संचित सकारात्मक शक्ति या पुण्य अन्यत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन इस सकारात्मक शक्ति को सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए, हमारे पास एक अत्यंत व्यापक और विस्तृत प्रेरणा और दृष्टिकोण होना आवश्यक है। यह केवल शिक्षाओं को सुनने वालों के लिए नहीं, बल्कि लामा या गुरु के लिए भी आवश्यक है।
पूर्णतः ज्ञानप्राप्त, करुणामय बुद्ध के शरीर में 32 प्रमुख और 80 गौण लक्षण हैं और उनकी वाणी में 60 ज्ञानवर्धक विशेषताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, उनका चित्त सभी अशांतकारी भावनाओं, मनोवृत्तियों और सभी आवरणों से मुक्त है, जिससे उन्हें शून्यता का, और साथ ही, सभी घटनाओं का, यथावत्, निर्वैचारिक प्रत्यक्ष ज्ञान सदैव प्रस्तुत रहता है। ऐसे करुणावान, पूर्णतः ज्ञानप्राप्त बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व यहीं बोधगया में अपने ज्ञानोदय का निदर्शन किया था और आज हम सब इसी स्थान पर हैं।
वर्तमान समय बहुत कठिन है, अनेक युद्ध, अकाल, आपदाएँ आदि हो रही हैं। फिर भी, हमारी पूर्व-संचित सकारात्मक शक्ति के कारण, हम ऐसे समय और स्थान पर जन्मे हैं और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, हमें शिक्षाओं और गुरुओं के साक्षात्कार के बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम जो ये शिक्षाएं सुन रहे हैं उनका हमें यथासंभव अभ्यास करना चाहिए।
हालाँकि, हम केवल कुछ पाने के लिए प्रार्थना करने को धर्म नहीं मान सकते। धर्म तो वह है जिसे हमें स्वयं आचरण में लाना है। यह केवल अपने मुख से कुछ शब्द बोलकर सुरक्षित दिशा (शरण) प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो हम कहते हैं उसे अपने दैनिक व्यवहार में लागू करना है। इसलिए, हमें शिक्षाओं में गहरी रुचि लेनी चाहिए और उनके समवेत अध्ययन और अभ्यास में स्वयं को शामिल करना चाहिए। लेकिन पहले यह जानना आवश्यक है कि यह कैसे किया जाए।
हम जितना अधिक धर्म से जुड़ते हैं, उतना ही अधिक सुखी होते हैं। यह हमारे द्वारा किए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों से उत्पन्न सकारात्मक शक्ति (पुण्य संचय) के संजाल के परिणामस्वरूप होता है। यही कारण है कि हमें केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अभ्यास से बुद्ध के अनुयायी बनने की आवश्यकता है। इससे अधिक सुख प्राप्त होगा। अतः, यहाँ बोधगया में, जहाँ हमें धर्म, और विशेष रूप से महायान धर्म से जुड़ने का अवसर प्राप्त है, यह महत्त्वपूर्ण है कि हम यथासंभव अधिक से अधिक सकारात्मक शक्ति का निर्माण करने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है एक उचित प्रेरणा निर्धारित करना। यदि हमारे पास एक व्यापक और अत्यंत सकारात्मक प्रेरणा है, तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम ऐसी प्रेरणा के बिना अभ्यास करते हैं, तो वह उतना प्रभावी नहीं होगा और बात नहीं बनेगी।
लामा के लिए भी यही बात लागू होनी चाहिए। लामा को अभिमान या प्रसिद्धि और सम्मान पाने के लिए, ईर्ष्या या दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा से शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बल्कि, उसकी एकमात्र प्रेरणा होनी चाहिए दूसरों का यथासंभव कल्याण, यहाँ उपस्थित सभी लोगों, सभी प्राणियों का सम्मान करते हुए, किसी को भी तुच्छ समझे बिना। श्रोताओं को भी अहंकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए ध्यानपूर्वक और सम्मानपूर्वक सुनना चाहिए। यदि लामा और शिष्य दोनों इस प्रकार उचित और सावधानीपूर्वक व्यवहार करें, तो यह अत्यंत लाभकारी होगा और हम सभी बहुत अधिक सकारात्मक शक्ति का निर्माण कर सकेंगे।
चाहे हमारे अंदर कितनी भी अशांतकारी भावनाएँ और मनोवृत्तियाँ हों, उनका समाधान करना और निराश न होना ज़रूरी है। ऐसा करने से, हम धीरे-धीरे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएँगे और अंततः उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। हम पाएँगे कि हर साल हम धीरे-धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। चूँकि चित्त स्वभावतः इन अशांतकारी भावनाओं और मनोवृत्तियों से कलंकित नहीं होता, इसलिए अगर हम अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए समर्पित कर दें, तो हम सफल हो सकते हैं। चूँकि हम जो दुख अनुभव करते हैं, वह हमारे चित्त के अनुशासित या वश में न होने के कारण होता है, इसलिए हमें इसका समाधान करना होगा। लेकिन यह सब एक साथ नहीं होगा।
उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बहुत ही उग्र और उद्दंड व्यक्ति को अधिक शांत और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इसमें कई वर्षों में धीरे-धीरे ही सफलता मिल सकती है। हमारे चित्त के साथ भी यही बात लागू होती है। हालाँकि हममें कमियाँ हैं, फिर भी हम धीरे-धीरे सुधार कर सकते हैं। हम बच्चों में भी यही देखते हैं। शुरुआत में, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता; वे पूरी तरह से निरक्षर होते हैं। लेकिन वे स्कूल में विभिन्न कक्षाओं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा इत्यादि से गुज़रते हैं, और अंततः इस क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से वे सीखते हैं और शिक्षित होते हैं। यही बात तब भी लागू होती है जब हम एक घर बनाते हैं, हम इसे मंज़िल दर मंज़िल बनाते हैं। हम इसे धीरे-धीरे करते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि इसमें कितना समय लगेगा, और जब तक हम कार्य पूरा नहीं कर लेते, तब तक विभिन्न चरणों से होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हमें अपने चित्त के साथ व्यवहार करते समय भी यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
जहाँ तक अपनी प्रेरणा निर्धारित करने की बात है, हमें अपने स्तर पर इसे यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए, और धीरे-धीरे हम लाम-रिम या "क्रमिक पथ" में वर्णित चरणों के माध्यम से इसे बेहतर बना पाएँगे। आप में से अधिकांश लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ नए लोगों के लिए मैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊँगा।
चित्त को वश में करना
धर्म का पालन करना केवल वस्र, पद या धन-संपत्ति बदलने की प्रक्रिया नहीं है। बल्कि इसका अर्थ है अपने दृष्टिकोण को बदलना और अपने चित्त को वश में करना। हम चाहे जो भी हों - यहाँ तक कि मैं, दलाई लामा भी - जब तक मेरा चित्त वश में नहीं हो जाता, मुझे धर्मावलंबी नहीं माना जा सकता। और हम किसी को केवल उसके नाम या उसके पहनावे के आधार पर ऐसा चित्त वाला नहीं कह सकते; बल्कि केवल उसकी वास्तविक मानसिक और भावनात्मक स्थिति के आधार पर कह सकते हैं। इसलिए, सबसे महत्त्वपूर्ण और निर्णायक बात अपने चित्त को वश में करना है।
यहाँ उपस्थित आप सभी को अपना परीक्षण करना होगा। हम सभी सुख चाहते हैं और कोई भी दुःख नहीं चाहता। हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिरदर्द होने पर उससे छुटकारा न चाहे। क्या ऐसा नहीं है? यह शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह के कष्टों के लिए सत्य है। लेकिन अनचाहे कष्टों को दूर करने और चित्तचाहा सुख प्राप्त करने में कई चरण होते हैं। यह सब एक साथ नहीं होता। यहाँ तक कि किसी पशु की मदद करने या उसे पालतू बनाने और उसे सुख पहुँचाने के प्रयास में भी, हमें उस पशु के अनुकूल चरणबद्ध रूप में काम करना होगा। उदाहरण के लिए, पहले हम उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, उसे डराने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने से बचते हैं, इत्यादि। यही बात हम पर भी लागू होती है, हमें चरणों में अपनी मदद करनी होगी।
सबसे पहले, हम इस आने वाले वर्ष या अगले वर्ष के लिए अपने लाभ के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। फिर अंततः हम अपने दायरे को बढ़ाकर बीस साल आगे की कल्पना करते हैं और फिर शायद अगले जन्म के लिए मानव जन्म प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इस आशा में कि हमें सुख मिलेगा और हमें लंबे समय तक दुख नहीं सहना पड़ेगा। हम ऐसे चरणों से गुज़रते हैं। इसलिए, अब जबकि हम मनुष्य हैं, आगे की सोचना बहुत ज़रूरी है और केवल अस्थायी, सतही स्तर पर नहीं, बल्कि परम सुख की प्राप्ति के लिए।
सुख की अपनी अधिक सामान्य खोज में, हम अपने शरीर के लिए भोजन, वस्र, आश्रय आदि खोजते हैं। लेकिन मनुष्य होने का उद्देश्य केवल यही नहीं है। भले ही हम धनवान हों, फिर भी हम पाते हैं कि धनी लोगों को भी मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। हम इसे पश्चिम में बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपार धन और भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, फिर भी उन्हें अवसाद, उलझन भरा चित्त और विभिन्न दयनीय अवस्थाओं जैसी अनेक मानसिक समस्याएँ भी हैं। बल्कि, हमने देखा है कि वहाँ बहुत से लोग इस स्थिति को सुधारने के लिए नशीले पदार्थ या दवाएँ लेते हैं। यह दर्शाता है कि यद्यपि उनके पास भौतिक सुख-सुविधाएँ और धन है, फिर भी वे अपने भौतिक सुखों के अतिरिक्त मानसिक सुख चाहते हैं, और केवल धन से ये दोनों नहीं मिलते। भले ही हम बहुत स्वस्थ और बलवान हों, यदि हमारा चित्त दुखी है तो यह पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के सुखों की आवश्यकता है। इनमें से चित्त अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह हम पर शासन करता है। इसलिए, चित्त की प्रसन्नता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
चित्त की प्रसन्नता उत्पन्न करना
लेकिन चित्त की यह प्रसन्नता कैसे आती है? यह हमारे विचारों के माध्यम से आती है। अगर हम अपने चित्त का प्रयोग करके नहीं सोचेंगे, तो हम खुद को प्रसन्नता नहीं दे पाएँगे। यह दोनों तरह से काम करता है। उदाहरण के लिए, चाहे हमारी सबसे प्रबल अशांतकारी भावनाएँ कोई भी हों, चाहे वह क्रोध हो, इच्छा हो, अभिमान हो, ईर्ष्या हो या कुछ और, हम जितना अधिक उनके बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक उनपर अमल करते हैं, और उतना ही अधिक दुख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर क्रोध हमारी सबसे प्रबल अशांतकारी भावना है, तो हम जितना अधिक क्रोधित होंगे, उतना ही अधिक दुखी होंगे।
उदाहरण के लिए, अगर हम तिब्बत को लेकर कटु और क्रोधित हैं, तो हम सुखी हैं या दुखी? हम दुखी हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए, इसके विपरीत, हमें प्रेम और करुणा के बारे में सोचना चाहिए। इससे हमारा क्रोध शांत होता है और चित्त को शांति मिलती है। इस प्रकार, एक सद्चित्त और दयालु विचार हमें सुख प्रदान करते हैं। चूँकि हम सभी इस सुख की कामना करते हैं और अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि इसका मूल चित्त है।
संक्षेप में, हमारी आसक्ति और द्वेष जितने प्रबल होंगे, हमारा दुख उतना ही प्रबल होगा। ये जितने कमज़ोर होंगे, हम उतने ही सुखी होंगे। इसलिए, हमें यह सोचना होगा कि हमें किन चीज़ों को दूर करना है, किन चीज़ों से अपने चित्त को मुक्त करना है। उदाहरण के लिए, अगर हम ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण हैं, तो क्या होगा? हम सभी को अंततः मरना ही है, इसलिए हम अपनी ईर्ष्या के स्रोतों को कभी भी बनाए नहीं रख पाएँगे। जैसे हम अपनी ईर्ष्यालु इच्छाओं को कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाएँगे, वैसे ही जब तक हम ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण रहेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएँगे। यही बात अभिमान पर भी लागू होती है। कोई भी हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रह सकता: हम हमेशा युवा और यौवनमय नहीं रह सकते। जिसपर हमें गर्व है, उसे हम अंततः खो देंगे। इस प्रकार, अभिमान भी चित्त की एक बहुत ही दुखभरी अवस्था है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में हैं और किसी और के स्वादिष्ट भोजन से ईर्ष्या करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें केवल दुःख ही मिलता है; इससे हमारा पेट बिल्कुल नहीं भरता!
अगर हम अपने बारे में सोचें, तिब्बतियों के बारे में, अगर हम चीनियों से नाराज़ और ईर्ष्यालु हों, तो क्या हम ऐसे सुखी हैं? क्या यह चित्त की एक सुखद स्थिति है? बिल्कुल नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसका जीवन का मुख्य कार्य अपने राग-द्वेषों को क्रियान्वित करना है। ऐसा व्यक्ति बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रसिद्ध हो सकता है; यहाँ तक कि इतिहास में भी दर्ज हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने क्या प्राप्त किया है? उसने तो बस इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वह सुखी नहीं हुआ है; वह मर चुका है। इसलिए अगर हम अपना पूरा जीवन अपने अशांतकारी मनोभावों को क्रियान्वित करने में बिता दें, तो चाहे हम कितने भी धनी और शक्तिशाली क्यों न हो जाएँ, इससे हमें सुख नहीं मिलेगा।
उदाहरण के लिए, अगर हम इन दिनों बोधगया में अपनी स्थिति के बारे में सोचें, तो हम इसे और भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ दलाई लामा के होते हुए भी, अगर आप इतने पवित्र स्थान पर हों और किसी भिखारी पर या कठिन भौतिक परिस्थितियों पर क्रोधित हो जाएँ, तो क्या आप उस समय खुश होते हैं? दूसरी ओर, जब आपके अशांतकारी मनोभाव कमज़ोर हों और आप यहाँ कुछ रचनात्मक कार्य कर रहे हों, तो क्या आप तब खुश होते हैं? ज़रा सोचिए।
आपकी मनःस्थिति आपके पड़ोसियों, मित्रों और बच्चों को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, एक पारिवारिक स्थिति पर विचार करें। यदि आप बहुत क्रोधित हैं और अपने बच्चों पर क्रोधित हो जाते हैं; आप उन्हें मारते हैं, वे रोते हैं - इससे सभी दुखी होते हैं, है न? लेकिन यदि आप क्रोधित नहीं हैं, यदि आप बहुत शांत हैं, तो आप बच्चों को खेलने देते हैं और सभी बहुत खुश और शांत रहते हैं। हमने देखा है कि यदि किसी देश में भी अनासक्त भाव और सहिष्णुता का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, तो उस स्थान के सुख में सभी लोग भागीदार होते हैं। यह बात व्यक्तियों, परिवारों और देशों पर भी लागू होती है। जितने अधिक अशांतकारी मनोभाव होते हैं, उतना ही अधिक दुख होता है; जबकि, जितने कम अशांतकारी मनोभाव होते हैं, उतना ही अधिक सुख होता है।
जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अशांतकारी मनोभावों और दृष्टिकोणों की हानि, उनसे होने वाली सभी बुराइयों, और उनके न होने के लाभों के बारे में काफ़ी सोचता हूँ। इससे मुझे अपने जीवन में अशांतकारी मनोभावों को कम करने पर ज़ोर देने में बहुत मदद मिलती है। फिर, एक अतिरिक्त लाभ के रूप में, हम पाते हैं कि हम जीवन का अधिक आनंद ले पाते हैं; हमारा भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है और सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन यदि हमारा चित्त अशांतकारी मनोभावों से भरा है, तो, चाहे हम ध्यान, पाठ या कुछ भी कर रहे हों, हमें उनसे कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए, हमें हमेशा यह सोचने का प्रयास करना चाहिए कि अशांतकारी मनोभाव कितने हानिकारक हैं।
संक्षेप में, यदि हमारा चित्त वश में है और हमारे चित्त में कोई अशांतकारी भावनाएँ या मनोवृत्तियाँ नहीं हैं, तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं। इसलिए, चित्त को वश में करने से जो सबसे अच्छी बात हो सकती है, वह यह है कि अशांतकारी भावनाएँ और मनोवृत्तियाँ उत्पन्न ही नहीं होंगी। लेकिन अगर वे उत्पन्न हो भी जाएँ, तो अगली सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन पर अमल न करें। उदाहरण के लिए, सबसे अच्छा यही है कि हम कभी क्रोधित ही न हों; लेकिन अगर हमारा गुस्सा भड़क जाए, तो हम पाते हैं कि अगर हम अपने चित्त को वश में कर चुके हैं, तो हम उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, हम किसी के मुँह पर मुक्का नहीं मारेंगे, उसे बुरा-भला नहीं कहेंगे, या ऐसी कोई भी अशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं करेंगे।
इस प्रकार धीरे-धीरे, एक क्रमिक प्रक्रिया में, हम पाते हैं कि प्रतिरोधी अधिकाधिक प्रबल होते जाते हैं, हमारा चित्त अधिकाधिक वश में होता जाता है और इस प्रकार हम अधिक सुखी होते जाते हैं। इसलिए, एक नवसाधक के रूप में, हमें प्रयास करना चाहिए कि क्रोध, आसक्ति आदि जैसे हमारे अशांतकारी मनोभाव कभी जाग्रत न हों। लेकिन यदि वे जाग्रत हों भी जाएँ, तो हमें उन्हें क्रियान्वित न करने का प्रयास करना चाहिए। आप समझ रहे हैं न? यदि हम अपने चित्त को वश में कर लेते हैं, तो यह धर्म का अभ्यास है, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते, तो वह धर्म नहीं है। यदि हम अशांतकारी मनोभावों को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, यदि हम निरोधसत्य (निरोध) या शांति की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो वास्तव में यही असली धर्म है।
चार आर्य सत्य
चार आर्य सत्य हैं: दुःखसत्य, उनके समुदयसत्य , सत्यनिरोध और सत्यचित्त मार्ग। दुःखसत्य के लिए, हम विभिन्न प्रकार के दुखों के बारे में सोच सकते हैं: मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा आदि। बुद्ध ने कहा था कि दुख के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस दुख का मूल क्या है? इसका मूल एक अदम्य चित्त है, और विशेष रूप से, यह अशांतकारी भावनाएँ और मनोवृत्तियाँ हैं। इसलिए, अशांतकारी भावनाओं और मनोवृत्तियों को दुःख का सच्चा कारण या वास्तविक स्रोत कहा जाता है, जैसा कि इन अशांतकारी भावनाओं के प्रभाव में उत्पन्न होने वाले कार्मिक आवेगों को भी कहा जाता है। इस प्रकार, अशांतकारी भावनाएँ और कर्म ही दुख के सच्चे कारण हैं। इसलिए, चूँकि हम सभी किसी भी दुख की कामना नहीं करते हैं और केवल उसे दूर करना चाहते हैं, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि इस दुख का कारण हमारा अदम्य चित्त है।
चूँकि हम उस दुख का सत्यनिरोध चाहते हैं ताकि वह फिर कभी उत्पन्न न हो, इसलिए हमें अपने अशांतकारी मनोभावों और दृष्टिकोणों को धर्मधातु या शून्यता के क्षेत्र में समाप्त करना होगा। इसे सत्यनिरोध का निर्वाण कहते हैं।
चूँकि अशांतकारी मनोभावों और प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने, या उन्हें हमेशा के लिए समाप्त करने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को आर्यों या महानुभावों का सत्यचित्त मार्ग कहा जाता है। अधिक सटीक रूप से, चूँकि विभिन्न अशांतकारी मनोभावों और प्रवृत्तियों को दूर करने की प्रक्रिया के दौरान, हम अधिक से अधिक गुणों को प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं, इसलिए वे चित्त जो एक ओर अशांतकारी मनोभावों और दोषों को दूर करते हैं और दूसरी ओर सद्गुणों को अर्जित करते हैं, उन्हें सत्यचित्त मार्ग कहा जाता है।
संक्षेप में, दुःखसत्य होता है; उसका समुदयसत्य होता है; हम उसके सत्यनिरोध की कामना करते हैं; और इसे साकार करने के लिए, हमें सत्यचित्त मार्ग को साकार करना होगा। इसका परिणाम एक निश्चित निरोध, शांति, या निर्वाण की स्थिति, "दुःख से परे अवस्था" की प्राप्ति है, और इससे हमें स्थायी सुख प्राप्त होता है। बुद्ध ने बोधगया में अपने उदाहरण से यही प्रदर्शित किया था, और उसके बाद उन्होंने चार आर्य सत्यों की शिक्षा दी थी। पहले दो, दुःखसत्य और उनके समुदयसत्य, मोह या अशुद्ध पक्ष के हैं, और दूसरे दो, सत्यनिरोध और सत्यचित्त मार्ग, मुक्तिदायक या शुद्ध पक्ष के हैं।
हम देख सकते हैं कि धर्म-साधना की प्रेरणा उस तरह नहीं है जैसे, उदाहरण के लिए, कोई बच्चा अपने माता-पिता की बात मानकर वैसा ही करता है जैसा उसे बताया जाता है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि माता-पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। धर्म-साधना का अर्थ सिर्फ़ एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने माता-पिता की बात मानना नहीं है। बल्कि, हम धर्म-साधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं और इसीलिए हम अपने चित्त को वश में करने के लिए गुरु द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं?
सर्वोच्च त्रिरत्न
दुखों के निवारण में कई कारक शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, भूख, सर्दी आदि के कष्ट हैं और इनमें से प्रत्येक के निवारण के लिए हम विभिन्न प्रकार के तरीकों या कार्यों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार, किसानों, व्यापारियों आदि के कार्यों के माध्यम से हम अपनी भूख और सर्दी का निवारण कर सकते हैं। बीमारी के कष्ट के लिए हम चिकित्सकों और दवाओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये केवल अस्थायी उपाय हैं, अंतिम इलाज नहीं। यदि हम बीमार हैं, तो हम सेहतमंद होने के लिए दवा ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे बुढ़ापे और मृत्यु को समाप्त नहीं करेंगी। संक्षेप में, हम जन्म, रोगों, बुढ़ापे और मृत्यु के कष्टों का अंतिम निवारण सामान्य तरीकों से नहीं कर सकते, भले ही कुछ उपाय हमें अस्थायी राहत दे दें।
कई धर्म, जैसे कि कुछ हिंदू संप्रदाय, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम, आदि, एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो सुख और दुख का रचयिता है। अगर हम इस ईश्वर से प्रार्थना करें, तो वह हमें सुख प्रदान करेगा। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं समझाया। बुद्ध ने कहा कि हमारे दुख और सुख ईश्वर के हाथ में नहीं, बल्कि पूरी तरह हमारे अपने हाथ में हैं।
उन धर्मों के विपरीत जो केवल एक शरण रत्न, अर्थात् ईश्वर, को स्वीकार करते हैं, हम तीन सर्वोच्च रत्नों को स्वीकार करते हैं। बुद्ध ही हैं जो हमें यह मार्ग दिखाते हैं कि क्या ग्रहण करना है और क्या अस्वीकार करना है। इसलिए, बुद्ध एक शिक्षक की तरह हैं, न कि किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की तरह। हमारे कर्म या व्यवहार ही हमारे सुख और दुख का निर्माण करते हैं। सुख सकारात्मक या रचनात्मक कार्यों से उत्पन्न होता है। इसलिए, हमें यथासंभव इसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर, चूँकि दुःख नकारात्मक विनाशकारी कार्यों से उत्पन्न होता है, इसलिए हमें यथासंभव उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
बुद्ध ने तब जो सिखाया वह कार्य-कारण का मार्ग था। हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है, न कि ईश्वर के, और न ही बुद्ध के। इस प्रकार, वास्तविक शरण या सुरक्षित दिशा धर्म में है, जिसे हमें अपने मानसिक सातत्यों पर विकसित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, अपने चित्त से अशांतकारी भावनाओं आदि को दूर करके, हम अपने दुखों का निवारण करेंगे और सुख प्राप्त करेंगे।
इसके अलावा, इस धर्म रत्न को अपने मानसिक सातत्यों पर विकसित करने के लिए, हमें ऐसे सहायकों की आवश्यकता होती है जो उदाहरण प्रस्तुत करें और इस प्रक्रिया में सहायता करें। ऐसे लोगों को संघ रत्न कहा जाता है।
संक्षेप में, बुद्ध हमें जीवन में सुरक्षित दिशा दिखाते हैं; धर्म ही वास्तविक सुरक्षित दिशा है; और संघ समुदाय इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसा कोई एक ईश्वर या शरण रत्न नहीं है जो हमें सुख दे और हमारे दुखों का निवारण करे।
विवेक और अभ्यास पर आधारित बौद्ध धर्म
अंग्रेज़ी में, "रिलीजन" शब्द का प्रयोग अक्सर तिब्बती शब्द "धर्म" के अनुवाद के लिए किया जाता है। धर्म शब्द का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार किया जाता है। इसलिए, आमतौर पर यह कहा जाता है कि बौद्ध धर्म नास्तिक है, और वास्तव में एक धर्म नहीं है। हालाँकि, चीनी कहते हैं कि वे नास्तिक हैं, बौद्ध धार्मिक हैं, और बौद्ध धर्म एक धर्म है। लेकिन वास्तव में, उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार, हम भी नास्तिक हैं।
इसके अलावा, हम बुद्ध के वचनों को अंधविश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी गहन जाँच के बाद ही स्वीकार करते हैं। अगर वे तर्कसंगत हैं, तो हम उन्हें स्वीकार करते हैं, और अगर नहीं, तो नहीं। उदाहरण के लिए, पुनर्जन्म जैसी घटनाओं के लिए हमारे पास कई तार्किक प्रमाण हैं और केवल उस विषय की जाँच के बाद ही हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई बात तर्क से स्थापित हो सकती है, तो वह स्वीकार्य है। लेकिन अगर वह केवल अंधविश्वास पर आधारित है; तो बात नहीं बनेगी। इसलिए, केवल "मैं विश्वास करता हूँ" मत कहिए। मुख्य बात तर्क और विवेक से विश्लेषण करना है। अगर कोई बात तर्क और वास्तविकता के अनुरूप नहीं है, तो उसे स्वीकार न करें। हमें अपने विश्वासों को हमेशा तर्क पर आधारित करना चाहिए।
अतीत में दिए गए बुद्ध के वक्तव्य उनकी सम्पूर्ण शिक्षाएँ हैं। उन्होंने जो कहा उसे संशोधित करने, उसमें कुछ जोड़ने या उसे सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल बुद्ध के उपदेशों का अभ्यास करना होगा। यह बहुत जटिल नहीं है। हम इसे चिकित्सा के उदाहरण से समझ सकते हैं। चिकित्सक प्रत्येक रोगी की जांच करते हैं और फिर प्रत्येक के लिए उपयुक्त दवा लिखते हैं। यदि उपचार काम नहीं करता है, तो केवल एक मूर्ख ही कहेगा कि दोष चिकित्सा विज्ञान में है। एक चतुर व्यक्ति यह समझ जाएगा कि दवा कारगर न होने का कारण न तो चिकित्सक है, न ही चिकित्सा विज्ञान। ठीक इसी प्रकार यह बौद्ध धर्म के सन्दर्भ में भी सत्य है। त्रिपिटक या तीन पिटक, बुद्ध की प्रत्यक्ष शिक्षाओं के ग्रंथ में कोई दोष नहीं हैं। यदि हम जांच करें, तो हम देखेंगे कि भ्रम मूल ग्रंथों में नहीं है। इसलिए आवश्यक यह है कि हम विभिन्न स्रोतों के निर्देशानुसार ठीक से अभ्यास करें। आप समझ गए?
महायान प्रेरणा की पुनः पुष्टि
मुख्य अभ्यास तो, चित्त को वश में करना है। इसके लिए हमें शिक्षाओं को सुनने की आवश्यकता है और इसे सही ढंग से करने के लिए, हमें एक सही प्रेरणा की आवश्यकता है। बुद्ध ने हीनयान और महायान, दोनों की शिक्षाएँ दीं। महायान में चित्त का मुख्य उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है। हीनयान में, इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि भले ही हम दूसरों की सहायता न कर सकें, लेकिन कम से कम हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इस प्रकार, दोनों में इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि कैसे दूसरों की सहायता की जाए और उनका भला कैसे किया जाए। हमें इससे सीख लेने की आवश्यकता है। अगर हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से हमें उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हमें किसी पर क्रोधित होना चाहिए, है न?
महायान की शिक्षाओं में यह भी कहा गया है कि हमें अपने स्वार्थों की परवाह किए बिना दूसरों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। यही बौद्ध धर्म का संदेश है, है न? इसलिए, हमें एक शुद्ध, स्नेही और दयालु हृदय रखने की आवश्यकता है। हमें बोधिचित्त संकल्प को अपनी प्रेरणा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा बोधिचित्त संकल्प सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु कार्य करना है। ऐसी प्रेरणा के साथ, अब बोधिसत्त्व तोग्मेज़ांगपो द्वारा लिखित 37 बोधिसत्त्व अभ्यासों को सुनें।
ग्रंथ के रचयिता की प्रमुख विशेषताएँ
तोग्मेज़ांगपो, बुतोन रिन्पोचे के समकालीन थे, जो त्सोंगखापा से दो पीढ़ी पहले की बात है। वे एक लामा थे, जो मुख्यतः शाक्य परंपरा में प्रशिक्षित थे और बचपन से ही दूसरों की मदद करने में रुचि रखने के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए, बचपन में, अगर लोग दूसरों की मदद नहीं करते थे, तो वे उन पर क्रोधित भी हो जाते थे। अंततः, वे एक भिक्षु बन गए और विभिन्न लामाओं, विशेषतः दो विशिष्ट गुरुओं पर आश्रित रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त की । उन्होंने सूत्र और तंत्र दोनों का अभ्यास किया और एक अत्यंत विद्वान, सिद्ध साधक बन गए।
वे बोधिचित्त के विकास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और यह उन्होंने मुख्यतः अपने आत्म को दूसरों के साथ रखने और उसका दूसरों के आत्म से आदान-प्रदान की शिक्षाओं के माध्यम से किया। वास्तव में, यदि हम किसी बोधिसत्त्व के बारे में सोचें, तो तोग्मेज़ांगपो का नाम तुरंत एक उदाहरण के रूप में चित्त में आता है, है न? वे ऐसे महान व्यक्ति थे, वास्तव में एक विशिष्ट व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए, जब भी कोई उनकी शिक्षाओं को सुनने आता, तो वे बहुत ही शांत, मौन और स्थिर हो जाते।
चूँकि उन्होंने हम सभी की सहायता के लिए इन सैंतीस अभ्यासों के बारे में लिखा था, इसलिए हमें इन शिक्षाओं का बार-बार परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। हम कहते हैं कि हम महायान के साधक हैं, लेकिन अगर हम हमेशा वास्तविक महायान अभ्यासों का परीक्षण नहीं करते, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए, हमें इन सैंतीस अभ्यासों के संदर्भ में स्वयं का परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वास्तव में हम अपने कार्यों को इनके अनुरूप करते हैं। इनमें, हमें प्रेरणा के तीन अलग-अलग स्तरों वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षाएँ मिलती हैं, जैसा कि लाम-रिम क्रमिक मार्ग में बताया गया है।
पाठ
अब मैं इस ग्रंथ पर एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। मुझे इसकी वंशावली कुनु लामा रिन्पोचे, तेनज़िन ग्यालत्सेन से प्राप्त हुई है, और उन्होंने इसे खाम प्रांत के पूर्व ज़ोग्चेन रिन्पोचे से प्राप्त किया था। यह केवल एक छोटा-सा पृष्ठभूमि इतिहास है और वास्तव में, यह प्रति मैं ल्हासा से अपने साथ लाया हूँ।
इन शिक्षाओं के स्रोत हैं शांतिदेव की बोधिसत्वचर्यावतार (संस्कृत - बोधिसत्वचर्यावतार), महायान सूत्रों के लिए मैत्रेय की महायानसूत्र-अलंकार (संस्कृत - महायानसूत्र-अलंकार), और नागार्जुन की रत्नावली (संस्कृत - रत्नावली)।
पाठ तीन भागों में बँटा हुआ है:
- आरंभ में, सकारात्मक बल का निर्माण
- वास्तविक शिक्षाएँ
- निष्कर्ष।
शुरुआत में, सकारात्मक शक्ति का निर्माण दो भागों में बँटा होता है:
- प्रारंभिक अभिवादन
- रचना करने की प्रतिज्ञा।
प्रारंभिक अभिवादन
यह पहला श्लोक इन दोनों खंडों में से पहला, प्रारंभिक अभिवादन प्रस्तुत करता है।
लोकेश्वर को प्रणाम।
मैं अपने तीनों द्वारों के माध्यम से, परम गुरुओं और संरक्षक अवलोकितेश्वर को सदैव सादर प्रणाम करता हूँ, जो यह जानते हुए कि सभी दृश्य-प्रपंचों का न आना है और न जाना, भटकते हुए प्राणियों के कल्याण के लिए अकेले ही प्रयास करते हैं।
अवलोकितेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिन्हें यहाँ लोकेश्वर कहा गया है। चूँकि आत्मज्ञान का मूल करुणा है, और चूँकि अवलोकितेश्वर उसके मूर्त रूप हैं, इसलिए यह साष्टांग प्रणाम उन्हीं को है। साथ ही, भविष्य में संस्कृत से परिचित होने और उसका अध्ययन करने के लिए हमें बीज और वृत्तियाँ प्रदान करने हेतु, लेखक ने संस्कृत में उनका नाम लोकेश्वर रखा है। यह साष्टांग प्रणाम अवलोकितेश्वर को गुरुओं से अभिन्न मानते हुए किया जाता है और यह शरीर, वाणी और चित्त के तीन द्वारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के साष्टांग प्रणाम का कारण ऐसी श्रद्धा की वस्तु के सद्गुण हैं।
ये सद्गुण क्या हैं? महायान का मूल बोधिचित्त लक्ष्य है। यह एक ऐसा चित्त है जो ज्ञानोदय की ओर उन्मुख है और जिसका उद्देश्य उसे प्राप्त करना है और ऐसा करके हम सभी सीमित जीवों का कल्याण कर सकते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, हमें छह व्यापक दृष्टिकोणों, छह पारमिताओं का अभ्यास करना होगा। परिणामस्वरूप, हम एक ऐसे ज्ञानोदय को प्राप्त कर पाते हैं जिसमें भौतिक और मानसिक दोनों पहलू होते हैं, अर्थात् रूपकाय और धर्मकाय या गहन जागरूक शरीर जो सब कुछ समाहित करता है, एक बुद्ध का सर्वज्ञ चित्त। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए, हमें उन कारणों का निर्माण करना होगा जो परिणामों के समान श्रेणियों में आते हैं। इस प्रकार, हमें बुद्ध के रूपकाय प्राप्त करने के लिए सकारात्मक शक्ति के एक जाल और बुद्ध के चित्त को प्राप्त करने के लिए गहन जागरूकता (ज्ञान का संग्रह) के एक जाल की आवश्यकता है। इनका आधार हैं दो सत्य।
लोकेश्वर वह हैं जो यह देखते हैं कि सभी घटनाओं का न तो कोई आना है और न ही कोई जाना। जब हम वस्तुओं के पारंपरिक सत्य की जाँच करते हैं, तो वस्तुएँ वास्तव में आती और जाती हैं। हालाँकि, यदि हम उनके बारे में गहनतम सत्य की जाँच करें, तो उनका आना और जाना वास्तविक और स्वाभाविक रूप से विद्यमान आने-जाने के रूप में स्थापित नहीं होता। उदाहरण के लिए, कार्य-कारण होता है। चूँकि कारणों का कोई अंतर्निहित अस्तित्व नहीं होता - वे अंतर्निहित अस्तित्व-रहित होते हैं - इसलिए उनके प्रभाव भी अस्तित्व के ऐसे असंभव तरीके से रहित होने चाहिए। न तो कारणों का और न ही प्रभावों का अंतर्निहित अस्तित्व होता है; वे एक-दूसरे पर निर्भर होने के रूप में स्थापित होते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी दृश्य-प्रपंचों की प्रतीत्यसमुत्पाद प्रकृति ग़ैर-अन्तर्निहित रूप से विद्यमान होने के रूप में स्थापित होती है।
जैसा कि नागार्जुन ने कहा है, वस्तुओं का कोई वास्तविक आगचित्त, प्रस्थान, स्थायीत्व आदि नहीं होता। इस प्रकार यह वाक्यांश कि, "यह देखना कि सभी दृश्य-प्रपंचों का कोई आगचित्त या प्रस्थान नहीं होता" शून्यता की ओर संकेत करता है और इस तथ्य की ओर कि यहाँ साष्टांग प्रणाम का विषय वह व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष निर्वैचारिक ज्ञान से शून्यता को समझता या देखता है। चूँकि प्रत्येक वस्तु आश्रित रूप से उत्पन्न होती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु अंतर्निहित अस्तित्व से रहित है। और चूँकि प्रत्येक वस्तु अंतर्निहित अस्तित्व से रहित है, इसलिए प्रत्येक वस्तु कार्य-कारण की प्रक्रिया द्वारा आश्रित रूप से उत्पन्न होती है।
यदि कारण अशांतकारी मनोभाव और प्रवृत्तियाँ हों, तो इनके परिणामस्वरूप दुख उत्पन्न होता है, और यदि कारण रचनात्मक कर्म हों, तो इनके परिणामस्वरूप सुख उत्पन्न होता है। चूँकि प्रतीत्यसमुत्पाद अशांतकारी मनोभावों और विनाशकारी कर्मों से उत्पन्न होता है, और यहाँ साष्टांग प्रणाम का उद्देश्य यह देखना है कि सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए उसकी करुणा केवल उन पर लक्षित है ताकि उन्हें उनके दुख को दूर करने का मार्ग दिखाने में मदद मिल सके। इस प्रकार, यहाँ ज्ञान और विधि दोनों पक्षों का संकेत दिया गया है क्योंकि बिना किसी एक के अभाव के, हमें दोनों की एक साथ आवश्यकता है।
इस हितकारी छंद से, हम इन दोनों पक्षों को देख सकते हैं। लोकेश्वर देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु अंतर्निहित सत्ता से रहित है और चूँकि प्रत्येक वस्तु शून्य है, इसलिए वे देखते हैं कि सभी दृश्य-प्रपंच कार्य-कारण से उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से, वे देखते हैं कि सभी प्राणियों का दुःख उनके अशांतकारी भावों और वृत्तियों से उत्पन्न होता है, और इसलिए वे करुणापूर्वक उस दुःख को दूर करने या उसे दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार, यहाँ लोकेश्वर के संबंध में ज्ञान और विधि के दोनों पक्षों की स्तुति की गई है। चूँकि वे प्रत्येक वस्तु को शून्य के रूप में देखते हैं, इसलिए वे प्रत्येक वस्तु को कार्य-कारण के रूप में देखते हैं। इस प्रकार, वे सभी के प्रति करुणा रखते हैं और उन्हें उनके दुःख से मुक्त करते हैं। क्या आप समझ पाए?
रचना करने का वचन
अगला श्लोक रचना करने का वचन है।
पूर्णतः प्रबुद्ध बुद्ध, जो लाभ और सुख के स्रोत हैं, पवित्र धर्म को साकार करने से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा, और चूँकि यह इस बात पर आधारित था कि वे इसके अभ्यासों को जानते थे, इसलिए मैं एक बोधिसत्त्व के अभ्यास का वर्णन करूँगा।
बुद्ध ने सर्वप्रथम बोधिचित्त का लक्ष्य विकसित किया ताकि सभी का कल्याण हो सके। फिर, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनका एकमात्र उद्देश्य रहा सभी का कल्याण करना। उन्होंने यह समझकर अपने चित्त को वश में किया कि उन्हें अपने सभी अशांतकारी मनोभावों और मनोवृत्तियों का उन्मूलन करना आवश्यक है और सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए सभी को यही करना आवश्यक है। इस प्रकार, बुद्ध ने इसके विभिन्न उपाय बताए और हमें उनके समान ही अभ्यास करना चाहिए। यदि हम उनके बताए अनुसार अभ्यास करें, तो हम भी सुख प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए, इस श्लोक में बुद्धजनों का लाभ और सुख के स्रोत के रूप में उल्लेख किया गया है।
बुद्ध स्वयं शुरू से ही आत्मज्ञानी नहीं थे। उन्होंने अपने गुरुओं पर भरोसा किया, उनकी शिक्षाओं का पालन किया और अपने चित्त को वश में किया। अपनी सभी अशांतकारी भावनाओं और मनोवृत्तियों को दूर करने की प्रक्रिया द्वारा, वे आत्मज्ञानी हो गए। इसलिए, उन्होंने पवित्र धर्म का अभ्यास करके और उसे साकार करके अपनी सिद्धि प्राप्त की।
हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास शरीर और चित्त दोनों किस प्रकार हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे चेतन नेत्र किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम यह नहीं कहते कि हमारे चेतन नेत्र उसे देखते हैं, बल्कि यह कहते हैं कि मैं स्वयं देखता हूँ। अगर हमारा शरीर बीमार हो जाता है, तो हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। इन अभिव्यक्तियों का अर्थ या तो यह है कि मैं एक सचेतन चित्त हूँ या मैं एक शरीर हूँ। लेकिन, हमारे शरीर सबसे पहले हमारी माताओं के गर्भ में बनते हैं और हमारी मृत्यु के साथ ही सड़ने पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए "मैं" सिर्फ़ एक शरीर नहीं हो सकता।
तो शायद, ऐसा हो कि मैं एक चित्त हूँ जो किसी शरीर पर निर्भर है। हालाँकि, "मैं" कोई रूप, आकार या रंग नहीं है। फिर भी, जब हम दूर से किसी शरीर को देखते हैं, तो उसके आधार पर हम कहते हैं, "ओह, मैंने अपने दोस्त को देखा" और हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो वह व्यक्ति सिर्फ़ उसका शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है, "क्या आपका शरीर ठीक है?" लेकिन ज़ाहिर है कि हम सिर्फ़ अपना शरीर नहीं हैं। अमेरिका में, कुछ प्रसिद्ध अस्पतालों में, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर लोगों को ध्यान-साधना का भी सुझाव देते हैं। इसलिए, ज़ाहिर है कि इस प्रकार का शरीर से इतर नुस्खा देने के लिए शरीर और चित्त के बीच कोई संबंध होना ज़रूरी है।
लेकिन इस "मैं" के चित्त होने का क्या अर्थ है? आइए चित्त की प्रकृति पर नज़र डालें। जब हम किसी वस्तु को जानते हैं, या किसी वस्तु के बारे में स्पष्ट या जागरूक होते हैं, तो हम कहते हैं, "मैं उस वस्तु को जानता हूँ।" लेकिन यह ठीक-ठीक पहचानना बहुत मुश्किल है कि चित्त क्या है। इसकी परिभाषा बस एक स्पष्टता और जागरूकता है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसका कोई रंग या आकार हो। अगर हम इसके बारे में सोचें, तो यह एक निर्मल स्थान जैसा है, एक बहुत ही खाली स्थान जहाँ सभी दृश्यमान इकाइयां समाप्त हो गई हैं और जहाँ किसी भी वस्तु का बोध उस निर्मल स्थान के भीतर केवल स्पष्ट और सचेतन रूप में उत्पन्न या प्रकट हो सका है।
चित्त, जो गर्भाधान के प्रथम क्षण में सूक्ष्म शरीर की वायु, बूँदों आदि के साथ-साथ उत्पन्न होता है, वह केवल स्पष्ट और सचेतन प्रकृति का होता है। ऐसी घटना के उत्पन्न होने के लिए, उसे अपने तात्कालिक कारण के रूप में किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जो उसी प्रकृति या उसी श्रेणी में विद्यमान हो जिसमें वह स्वयं है। इसलिए, गर्भाधान के क्षण में स्पष्टता और सचेतनता के प्रथम क्षण के लिए कारण के रूप में कार्य करने हेतु केवल स्पष्टता और सचेतनता के एक पूर्व क्षण का होना आवश्यक है। इसी तर्क के आधार पर हम पूर्वजन्मों के अस्तित्व को स्थापित या सिद्ध करते हैं। और यदि पूर्वजन्मों का अस्तित्व है, तो इसका अर्थ है कि भविष्य के जन्मों का भी अस्तित्व होगा।
चूँकि हमारे पास जो स्पष्टता और सचेतनता है, वह निरन्तरता में है और भविष्य के जन्मों में भी बनी रहेगी, इसलिए इस पर छाए उन अवरोधों या आवरणों को हटाना अत्यंत आवश्यक है जो हमारी विभिन्न अशांतकारी भावनाओं और कष्टों का कारण बनते हैं। इन्हें हटाकर, हम चेतना के स्वाभाविक आधार तक पहुँचने में सक्षम हो जाते हैं, जो केवल अनवरुद्ध स्पष्टता और सचेतनता है। यही एक बुद्ध, एक पूर्णतः ज्ञानप्राप्त सत्त्व का सर्वज्ञ चित्त बन सकता है। अतः, चूँकि हमारे अपने चित्त और एक ज्ञानप्राप्त सत्व, या एक सर्वज्ञ चित्त, का आधार एक ही है, इसलिए इस प्रकार का चित्त हम स्वयं निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। एक बुद्ध वह व्यक्ति नहीं है जो शुरू से ही प्रबुद्ध हो; वह विभिन्न कारणों पर निर्भर होकर प्रबुद्ध हुआ। उसने स्वयं को उन चीज़ों से मुक्त (त्याग) किया जिनसे छुटकारा पाना आवश्यक था और जो प्राप्त करना आवश्यक था, उसे प्राप्त किया। इसलिए, यदि हम भी ऐसा ही करें, तो हम भी उसे प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार, ग्रंथ कहता है, "पूर्णतः प्रबुद्ध बुद्ध, लाभ और सुख के स्रोत, ज्योतिवलयित धर्म को साकार करने से उत्पन्न हुए हैं।" हम स्वयं ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें कहा गया है, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे इसके अभ्यासों को जानते थे।" अतः, केवल धर्म के बारे में जानना ही पर्याप्त नहीं है। धर्म के अभ्यासों को जानने के बाद, उन्हें व्यवहार में लाना और साकार करना आवश्यक है।
मैं आज के लिए यह पाठ यहीं छोड़ता हूँ। क्या आप सब कुछ समझ गए? हमें जितना हो सके उतना अभ्यास करना चाहिए। हमें त्याग, बोधिचित्त और शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। हमें स्वयं को बहुत ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से परखना चाहिए, यह देखना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रवृत्तियाँ और रुझान क्या हैं, और फिर अपने अनुकूल मार्ग पर स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए।